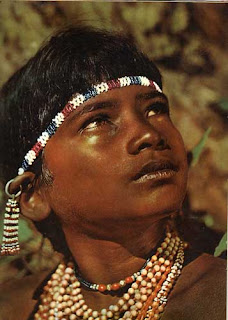इस बात को साल भर से अधिक हो गया। मैंने बस्तर में जारी नक्सलवाद के खिलाफ किसी लेख में टिप्पणी की थी। उस दिन मेरे नाम को इंगित करते हुए एक पोस्ट “मोहल्ला” ब्लॉग पर डाली जिसका शीर्षक था – “बस्तर के हो तो क्या कुछ भी कहोगे?” और लिंक - http://mohalla.blogspot.com/2008/05/blog-post_24.html इस पोस्ट नें मुझे झकझोर दिया। मैं माओवाद को ले कर हो रहे प्रचार की ताकत जानता हूँ और चूंकि मेरा अपना घर जल रहा हैं इस लिये आतंकवाद और क्रांति जैसे शब्दों के मायने भी समझने लगा हूँ। मैंनें निश्चित किया कि बस्तर का एक और चेहरा है जो माओवाद और सलवाजुडुम की धाय धमक में कहीं छुप गया है। बस्तर की और भी तस्वीरें हैं जो लाल नहीं हैं और बस्तर वैसा तो हर्गिज नहीं जो अरुन्धति के आउटलुक से दिखाया गया। अपनी मातृभूमि बस्तर के लिये कहानियाँ, आलेख और संस्मरण लिखते हुए अचानक ही एक उपन्यास लिखने का विचार कौंधा। बस्तर के इतिहास और वर्तमान पर काम करने का फिर मुझमें जुनून सा सवार हुआ। मैंने केवल शोध के कार्य के लिये बस्तर भर की कई यात्रायें कीं और उन जगहों पर विशेष रूप से गया जहाँ जाना इन दिनों दुस्साहस कहा जाता है। यानि कि हम अपने ही घर, अपनी ही मिट्टी में निर्भीक नहीं घूम सकते?
मेरे बस्तर विषयक आलेख जब पत्र-पत्रिकाओं और ब्ळोग में प्रकाशित होने लगे तो मेरा दो तरह के स्वर से सामना हुआ। पहला स्वर जो मुझसे सहमत था और दूसरा जो असहमत। असहमति भी स्वाभाविक है, मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि मेरी तरह ही सभी सोचें। सब एक तरह ही सोचते तो भी समाजवाद होता? लेकिन जो बात सबसे अधिक विचारणीय है वह है सोच की खेमेबाजी, सोच का रंग और सोच का झंडा। कोई तर्क करे तो समझ में आता है, कोई विचार रखे और उद्धरण दे तो भी समझ में आता है यहाँ तक कि किसी के अनुभव सामने आयें वह विरोधाभासी भी हों तो भी सोच को जमीन देते हैं। लेकिन “खास तरह के खेमेबाजों का” एक मजेदार विश्लेषण है – आप वामपंथी नहीं हो तो आप संघी हो या दक्षिणपंथी हो?
मैं बहुत सोचता हूँ कि आखिर क्या हूँ मैं? उम्र के पन्द्रह साल से ले कर लगभग सत्ताईस साल तक अपने नाम के आगे कामरेड सुनना अच्छा लगता था। इप्टा से जुड कर में नुक्कड भी किये, गली गली जनगीत भी गाये, हल्ला भी बोला इतना ही नहीं उस दौर के लिखे हुए मेरे अनेकों नाटक लाल सुबह ही उगाते हैं जिनमें प्रमुख हैं – किसके हाँथ लगाम, खबरदार एक दिन, और सुबह हो गयी आदि आदि। किसके हाँथ लगाम की एक प्रस्तुति ‘भारत-भवन’ में तथा मेरे नाटकों की कई प्रस्तुतियाँ भोपाल के रवीन्द्र भवन में भी हुई हैं। तब की लिखी मेरी कहानियों के अंत में हमेशा ही लाल सुबह होती रही थी। लेकिन बहुत कुछ तब दरका जब तू चल मैं आया वाले प्रधानमंत्रियों का दौर आया और वामपंथी दलों की अवसरवादिता नें मेरे सिद्धांतों की कट्टरता को झकझोर दिया। धर्म को जनता की अफीम मानने वाले एक दिवंगत कामरेड की पहचान हमेशा उनकी पगडी से ही रही। पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ लडने वाले कई छत्रप अपने बेटों के लिये लाल कालीन की जुगाड में ही दिखे। उनका श्रम भी रंग लाया और कुछ फैक्ट्री मालिक है तो कुछ सी.ई.ओ। मैं धीरे धीरे प्रायोजित विरोध और स्वाभाविक विरोध के अंतर को समझने लगा हूँ।
एसे ही एक दिन जब मैं अपने घर बचेली पहुँचा तो अपनी डायरी ले कर जंगल जाने लगा। जंगल में सिम्प्लेक्स नाले पर एक पत्थर मेरी टेबल-कुर्सी दसियों साल से ‘था’। यहाँ पानी में पैर डाले घंटों अपनी किताबों के साथ मैं समय गुजारा करता था। दसवी और बारहवी में अपने प्रिपरेशन लीव के दौरान भी मैं यहीं सारे सारे दिन बैठ कर पढा करता था। यहीं मैने कई वो कहानियाँ और नाटक भी लिखे जिनके अंत में मुक्के तन जाने के बाद धरती समतल हो गयी और एक सी धूप फैल गयी। इस बार जब मम्मी नें जंगल में उस ओर जाने से रोक दिया। कारण था नक्सलवाद। एसा प्रतीत हुआ जैसे किसी नें मुझे मेरे ही घर में घुसने से रोक दिया। उस दिन मैने गहरे सोचा कि एसा क्यों है कि मैं उदास हूँ? मुझे तो खुश होना चाहिये था कि वैसा ही हो रहा है जैसा मेरी कहानियों में होता था कि क्रांतिकारी बंदूख ले कर उग आये हैं और ढकेल कर लाल सवेरा के कर आने ही वाले हैं? मैंने अपनी कहानियों को टटोला लेकिन उनमें कहीं बारूदी सुरंग फाड कर सुकारू और हिडमाओं की ही लाशों के अनगिनत टुकडे किये जाने की कल्पना नहीं थी। मैंने जब भी क्रांतिकारी सोचे तो वो भगतसिंह थे। उनकी नैतिकता एसी थी कि असेम्बली में भी बम फेंके तो यह देख कर कि कोई आहत न हो लेकिन बात पहुँच जाये। बस्तर के इन जंगलों में जो धमाके रात दिन हो रहे हैं क्या ये बहरों को सुनाने के लिये हैं? नहीं ये अंधों की लगायी आग है और दावानल बन गयी हैं। ये सब कुछ जला देगी खेत-खलिहान भी, महुआ-सागवान भी, आदिम किसान भी।
नहीं मैं लाल नहीं सोचता, हरा नहीं सोचता, भगवा नहीं सोचता, नीला पीला या काला कुछ नहीं सोचता। मेरी सोच को मेरी लिये बख्श दो भाई। चूल्हे में जायें सारे झंडे और सारे नारे। तुम उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, साम, दाम, वाम जो भी हो मुझे ये गालिया न दो। मैने बहुत सी कहानिया जला दी हैं बहुत से नाटक अलमारी में दफन कर दिये हैं और अब मैं वही लिखता हूँ जो मैं खुद सोचता हूँ अपने बस्तर के लिये।